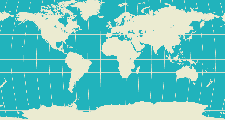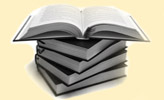प्रौद्योगिकिओं पर आधारित उत्पादकता के बड़े लाभ
 भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्वर्ण जयंती
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्वर्ण जयंती
स्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि उनकी सरकार ने सदा स्वीकार किया है कि समृद्ध, उत्पादक और टिकाऊ कृषिगत अर्थव्यवस्था हमारे देश के न्यायसंगत और समावेशी विकास का आधार है, इसलिए हमने एक व्यापक सुधार और कृषिगत अर्थव्यवस्था के उन्नयन की नीतियों का अनुसरण किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने खेती से आमदनी में सुधार के लिए और ग्रामीण बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने की बहु-आयामी नीति अपनाई है, हमारे फ्लैगशिप कार्यक्रम ने ग्रामीण सड़कों, ग्रामीण विद्युतीकरण, सिंचाई, ग्रामीण आवास और ग्रामीण संचार में निवेश बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है।
मनमोहन सिंह ने कहा कि इन नीतियों के सार्थक परिणाम नजर आने लगे हैं, हम खाद्यान्न उत्पादन में नई उंचाइयों पर पहुंच गये हैं, ग्याहरवीं योजना के अंत में खाद्यान्न उत्पादन 250 मिलियन टन को पार कर जायेगा, जो सर्वकालिक रिकॉर्ड है, दलहन का 18 मिलियन टन का उत्पादन पिछले 15 मिलियन टन से कहीं अधिक है, हम आज अधिक दूध, अधिक फल, अधिक सब्जियां, अधिक गन्ना, अधिक तिलहन और पहले से कहीं अधिक कपास पैदा कर रहे हैं, पिछले वर्ष सब्जियों के उत्पादन में 9.57 प्रतिशत वृद्धि हुई और लगभग दो मिलियन टन शीत भंडारण की क्षमता तैयार की गई। उन्होंने कहा कि अब ऐसा प्रतीत होता है कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि विकास लगभग 3.5 प्रतिशत प्रति वर्ष रहेगा, जो कि दसवीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में कहीं बेहतर है, यह एक सराहनीय उपलब्धि है, लेकिन हमें बारहवीं योजना में इसे और सुधारना होगा ताकि कृषि विकास चार प्रतिशत अथवा उससे कहीं अधिक पहुंच जाये। इसके लिए दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को विभिन्न क्षेत्रों में संकल्प लेकर प्रयास करने होंगे, जिनमें कृषि में निवेश, जल संरक्षण प्रबंधन, विपणन समर्थन और ऋण का प्रावधान आदि शामिल हैं। उस प्रयास में एक मुख्य तत्व कृषि अनुसंधान का योगदान होना चाहिए।
प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली को आगामी वर्षों की चुनौतियों का सामना करने के लिए और सुदृढ करने की आवश्यकता है। इस बारे में हमारी आवश्यकता वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने की है। हमारी सरकार लगभग एक प्रतिशत के वर्तमान स्तर से बारहवीं योजना के अंत तक अनुसंधान और विकास पर खर्च सकल घरेलू उत्पाद के कम से कम दो प्रतिशत बढ़ाने के लिए वचनबद्ध है। कृषि संबंधी हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों के महत्व को ध्यान में रखते हुए हमें सुनिश्चित करना है कि अनुसंधान और विकास पर बढ़े हुए परिव्यय का एक बड़ा हिस्सा कृषि और सबद्ध गतिविधियों पर खर्च हो। उन्होंने कहा कि संसाधन, समाधान का मात्र एक अंग है, हमने इस प्रणाली की जांच करने और उसे सुदृढ़ करने के तौर-तरीके सुझाने के लिए दो समितियां गठित की थीं, एक समिति की अध्यक्षता डॉ मशलकर ने और दूसरे की डॉ स्वामीनाथन ने की। हमें इन समितियों की सिफारिशों के कार्यान्वयन की यह जानने के लिए समीक्षा करने की आवश्यकता है कि उनकी सभी सिफारिशें अक्षरश: कार्यान्वित हों।
उन्होंने कहा कि अनुसंधान परिव्यय स्पष्ट रूप से परिभाषित अनुसंधान लक्ष्यों पर आधारित हों, जो इस क्षेत्र में उत्पादकता वृद्धि प्राप्त करने से जुड़े हैं। इसके लिए एक प्रणाली बनाने की आवश्यकता है, जो एक ओर तो आधारभूत अनुसंधान पर ध्यान केन्द्रित करे और दूसरी ओर विभिन्न क़िस्मों के विकास के लिए बुनियादी अनुसंधान को साकार रूप देने वाली उन गतिविधियों के स्पैक्ट्रम को प्रोत्साहित करे, जो हमारे किसानों की आवश्यकताओं को उनकी परिस्थितियों और संसाधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए पूरा करे। उन्होंने कहा कि नि:संदेह सार्वजनिक क्षेत्र को इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए, वास्तव में, जब तक निजी क्षेत्र परिव्यय का एक बड़ा हिस्सा नहीं लगाता तब तक अनुसंधान में सकल घरेलू उत्पाद के दो प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त करना संभव नहीं है, साथ ही, हमारी अर्थव्यवस्था के कृषि, औद्योगिक और विज्ञान एवं प्रौद्योगिक क्षेत्रों में अत्यधिक समन्वय से नई अभिनवताओं और प्रौद्योगिकिओं पर आधारित उत्पादकता के बड़े लाभ प्राप्त किये जा सकते है।
उन्होंने कहा कि हमें संस्थाओं और व्यवस्थाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने के लिए ढांचागत सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, तथापि, इसे बड़े स्तर पर घटित करने के लिए हमें मात्र संस्थाओं के लिए धन उपलब्ध करने तक नहीं बल्कि संस्थाओं के लिए अनुसंधान मंच तैयार करके वैज्ञानिक अनुसंधान के तौर-तरीकों का विस्तार करने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ताओं और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली, विश्वविद्यालयों, सीएसआईआर, वैज्ञानिक संस्थानों अथवा निजी क्षेत्र के अनुसंधान समूहों को मुख्य वरियता क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान के लिए मंच तैयार करने में सक्षम बनाना चाहिए, इनके लिए धन जुटाया जाना चाहिए लेकिन इनकी उच्च स्तर पर समीक्षा भी की जानी चाहिए, इसलिए कृषि अनुसंधान परिषद ने बारहवीं योजना में इस दिशा में कुछ अधिक म्यूरल परिव्यय का प्रस्ताव किया है।
उन्होंने कहा कि भविष्य में हमें न केवल खाद्यान्न की मांग में वृद्धि को बल्कि उस मांग के बदलते हुए स्वरूप को भी ध्यान में रखना है। अनुमान है कि अगले दस वर्षों में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त लगभग पचास मिलियन टन खाद्यान्न की आवश्यकता होगी। खाद्यान्न का अधिक उत्पादन निश्चित रूप से खाद्य सुरक्षा का और देश को कुपोषण के अभिशाप से मुक्ति दिलाने के हमारे प्रयासों का एक महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने कहा कि समुचित पौष्टिकता के लिए संतुलित भोजन की आवश्यकता है, हमें फल और सब्जियां तथा प्रोटीन युक्त उत्पाद जैसे दूध, अंडे, मछली और मांस अधिक पैदा करने की आवश्यकता है। इन उत्पादों की मांग भी बढ़ती हुई आमदनी और भोजन की बदलती हुई आदतों तथा प्राथमिकताओं के साथ पर्याप्त बढ़ने की आशा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने पहले ही जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने की आवश्यकता का उल्लेख किया है। जलवायु परिवर्तन और व्यावसायिक ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग का भारत में कृषि पर अत्यधिक प्रभाव पड़ने की आशा है। ऊर्जा की मांग में वृद्धि और जीवाश्म–ईंधन आधारित ऊर्जा पर निरंतर निर्भरता के कारण खेती की कीमतें बढ़ेंगी और कार्बन उत्सर्जन की भी वृद्धि होगी। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इन समस्याओं से निपटने के लिए आईएआरआई ने हाल ही में पर्यावरण विज्ञान और जलवायु आधारित कृषि के लिए एक नये केंद्र की स्थापना की है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जैसी संस्थाओं के यशस्वी इतिहास और इसमें आज प्रशिक्षित किए जा रहे युवा मस्तिष्कों की गुणवत्ता से पता चलता है कि हमारे पास इन चुनौतियों का सामना करने के लिए कुशाग्र और संस्थागत क्षमता है। उन्होंने डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए जीवन में सफलता की कामना की।

 मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश