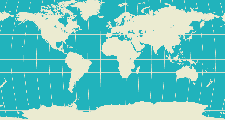
а§≤а§≤а§Ъৌ১а•З а§≠а§∞ুৌ১а•З а§З৴а•Н১ড়৺ৌа§∞
৙а§≤а•На§≤৵а•А ৙а•На§∞а§Хৌ৴
Wednesday 13 March 2013 03:54:58 AM

а§Жа§Іа•Б৮ড়а§Х а§ѓа•Ба§Ч а§Ѓа•За§В а§Ха§ња§Єа•А а§≠а•А а§Й১а•Н৙ৌ৶ а§Ха•А ৵а•Нৃ৵৪ৌৃড়а§Х а§Єа§Ђа§≤১ৌ а§Ха•З а§≤а§ња§П ৵ড়а§Ьа•На§Юৌ৙৮ а§Ьа§∞а•Ба§∞а•А ৐৮ а§Ча§П а§єа•Иа§Ва•§ ৵ড়а§Ьа•На§Юৌ৙৮а•Ла§В а§Ха§Њ а§Ѓа•Ба§Ца•На§ѓ а§Ха§Ња§∞а•На§ѓ а§ђа§Ња§Ьа§Ља§Ња§∞ а§Ѓа•За§В а§Ж а§∞а§єа•З а§Й১а•Н৙ৌ৶а•Ла§В а§Ха•З ৵ড়ৣৃ а§Ѓа•За§В а§Й৙а§≠а•Ла§Ха•Н১ৌ а§Ха•Л ু৺১а•Н৵৙а•Ва§∞а•На§£ а§Ьৌ৮а§Ха§Ња§∞а•А а§Й৙а§≤а§ђа•НвАНа§І а§Ха§∞ৌ৮а•З а§Ха•З ৪ৌ৕ а§єа•А а§Ха§ња§Єа•А а§Ца§Ња§Є а§Ха§В৙৮а•А а§Ха•З а§Й১а•Н৙ৌ৶ а§Ха•З а§ђа§Ња§∞а•З а§Ѓа•За§В а§Й৙а§≠а•Ла§Ха•Н১ৌ а§Ха•А ৵ীৌ৶ৌа§∞а•А а§Ха•Л ৐৮ৌа§П а§∞а§Ц৮ৌ а§≠а•А а§єа•И, ১ৌа§Ха§њ ৵৺ а§ђа§Ња§∞-а§ђа§Ња§∞ а§Йа§Єа•А а§Ха§В৙৮а•А а§Ха•З а§Й১а•Н৙ৌ৶ а§Ца§∞а•А৶а•За•§ ৶а•Ва§Єа§∞а•З ৴৐а•Н৶а•Ла§В а§Ѓа•За§В ৵ড়а§Ьа•На§Юৌ৙৮, а§Й১а•Н৙ৌ৶а§Х а§Фа§∞ а§Й৙а§≠а•Ла§Ха•Н১ৌ а§Ха•З а§ђа•Аа§Ъ а§Єа§В৵ৌ৶ а§Ха•А ৵৺ ৙а•На§∞а§Ха•На§∞а§ња§ѓа§Њ а§Жа§∞а§Ва§≠ а§Ха§∞১а•З а§єа•Иа§В, а§Ьа§ња§Єа§Ѓа•За§В ৵ড়а§≠ড়৮а•Н৮ а§Єа§Ња§Ѓа§Ња§Ьа§ња§Х а§Фа§∞ а§Жа§∞а•Н৕ড়а§Х а§Ха§Ња§∞а§Х а§≠а•А ৮ড়৺ড়১ а§єа•Л১а•З а§єа•Иа§Ва•§ ৵ড়а§Ьа•На§Юৌ৙৮а•Ла§В а§Ха•А а§Єа§∞а•Н৵৵а•Нৃৌ৙а§Х১ৌ а§Жа§Ь ৵ড়৴а•Н৵ а§Ха•З а§Жа§∞а•Н৕ড়а§Х ৙а§∞ড়৶а•Г৴а•На§ѓ а§Ѓа•За§В а§Ж а§∞а§єа•З ৐৶а§≤ৌ৵ а§Єа•З а§≠а•А а§Єа§Ва§ђа§В৲ড়১ а§єа•Иа•§ а§ђа•А৪৵а•Аа§В ৪৶а•А а§Ха•З а§Еа§В১ড়ু ৶৴а§Х а§Ѓа•За§В а§Єа§В৙а•Ва§∞а•На§£ ৵ড়৴а•Н৵ а§Ѓа•За§В а§Єа§Ѓа§Ња§Ь৵ৌ৶а•А ৵а•Нৃ৵৪а•НвАН৕ৌа§Уа§В а§Ха•З ৵ড়а§Ша§Я৮ ৮а•З а§Єа§Ва§Ч৆ড়১ ৙а•Ва§Ва§Ьа•А৵ৌ৶ а§Ха•Л а§Ѓа§Ьа§ђа•В১а•А ৙а•На§∞৶ৌ৮ а§Ха•А а§єа•Иа•§ а§За§Є а§Єа§Ва§Ч৆ড়১ ৙а•Ва§Ва§Ьа•А৵ৌ৶ ৮а•З а§Ьа§ња§Є а§≠а•Ва§Ѓа§Ва§°а§≤а•Аа§Ха§∞а§£ а§Ха•Л ৵а•И৴а•Н৵ড়а§Х ৙а§∞ড়৶а•Г৴а•На§ѓ ৙а§∞ ৙а•На§∞а§Єа•Н১а•Б১ а§Ха§ња§ѓа§Њ, ৵৺а•А а§Й৙а§≠а•Ла§Ха•Н১ৌ৵ৌ৶а•А а§Єа§Ва§Єа•На§Ха•Г১ড় а§Ха•З ৙а•На§∞а§Ъа§Ња§∞ а§Фа§∞ ৙а•На§∞а§Єа§Ња§∞ а§Ѓа•За§В а§Еа§єа§Ѓ а§≠а•Ва§Ѓа§ња§Ха§Њ ৮ড়а§≠а§Њ а§∞а§єа•З а§єа•Иа§Ва•§
а§≠а•Ва§Ѓа§Ва§°а§≤а•Аа§Ха§∞а§£ а§Єа•З ৙৺а§≤а•З а§Ха•З ৵ড়а§Ьа•На§Юৌ৙৮а•Ла§В а§Ха•Л а§Еа§Ча§∞ а§Ча•Ма§∞ а§Єа•З ৶а•За§Ца•За§В ১а•Л а§Ра§Єа§Њ а§≤а§Ч১ৌ а§єа•И а§Ха§њ а§Йа§Є ৶а•Ма§∞ а§Ѓа•За§В ৵ড়а§Ьа•На§Юৌ৙৮ а§Ха§Ња§Ђа•А ৺৶ ১а§Х а§Єа§Ња§Ѓа§Ња§Ьа§ња§Х а§∞а•В৙ а§Єа•З а§Єа§єа•А, а§Фа§Ъড়১а•Нৃ৙а•Ва§∞а•На§£ а§Фа§∞ ৙а•Ва§∞а•Н৵ৌ৮а•Бুৌ৮ড়১ а§єа•Л১а•З ৕а•З, а§≤а•За§Хড়৮ а§Жа§Ь а§Ха•З ৵ড়а§Ьа•На§Юৌ৙৮ а§єа§Ѓа§Ња§∞а•А а§Єа•Ла§Ъ а§Ха•З а§≤а§ња§П а§Ха•Ла§И а§Е৵а§Хৌ৴ ৮৺а•Аа§В а§Ыа•Лৰ৊১а•За•§ ৵ড়а§Ьа•На§Юৌ৙৮ а§єа•А а§ѓа§є ১ৃ а§Ха§∞৮ৌ а§Ъৌ৺১а•З а§єа•Иа§В а§Ха§њ а§єа§Ѓ а§Ха•На§ѓа§Њ а§Ца§Ња§Па§В, а§Ха•На§ѓа§Њ ৙ড়а§Па§В а§Фа§∞ а§Ха•На§ѓа§Њ ৙৺৮а•За§В? а§Ха§ња§Єа•А а§Ца§Ња§Є а§Ђа•За§ѓа§∞৮а•За§Є а§Ха•На§∞а•Аа§Ѓ а§Ха•З а§За§Єа•Н১а•За§Ѓа§Ња§≤ а§Єа•З а§Ха•Ла§И а§≤а§°а§Ља§Ха•А а§Е৙৮а•З вАШ৙а•На§∞а§ња§Ва§Є а§Ъа§Ња§∞а•На§Ѓа§ња§Ва§ЧвАЩ а§Ха•Л ৙ৌ а§Єа§Х১а•А, ১а•Л а§Ха§ња§Єа•А а§Ца§Ња§Є а§°а§ња§ѓа•Ла§°а§∞а•За§Ва§Я а§ѓа§Њ а§Жа§Ђа•На§Яа§∞ ৴а•З৵ а§Ха•З а§За§Єа•Н১а•За§Ѓа§Ња§≤ а§Єа•З а§Ха•Ла§И ৙а•Ба§∞а•Ва§Ј а§Е৙৮а•А а§°а•На§∞а•Аа§Ѓ а§Ча§∞а•На§≤ а§Ха•Ла•§ а§Ѓа§Ња§В а§Фа§∞ а§ђа§Ъа•На§Ъа•З а§Ха•З а§ђа•Аа§Ъ ৙а•На§ѓа§Ња§∞ ৐৥৊ৌ৮ৌ а§єа•Л ১а•Л а§Ѓа•Иа§Ча•А, ৮а•Ва§°а§≤а•На§Є а§Фа§∞ ৮а•Йа§∞ а§Єа•В৙ а§Ха§Ња§Ѓ а§Ж১а•З а§єа•Иа§В а§Фа§∞ ৙а•На§∞а•За§Ѓа•А-৙а•На§∞а•За§Ѓа§ња§Ха§Њ, а§Ьа•Л а§Єа§Ња§Ва§Є а§ѓа§Њ ৐৶৮ а§Ха•А ৶а•Ба§∞а•На§Ча§Ва§І а§Ха•А ৵а§Ьа§є а§Єа•З ৶а•Ва§∞ а§єа•Л а§Ьৌ১а•З а§єа•Иа§В, а§Ха§ња§Єа•А а§Ца§Ња§Є а§Яа•В৕৙а•За§Єа•На§Я а§ѓа§Њ а§°а§ња§ѓа•Ла§°а§∞а•За§Ва§Я а§Ха•А ু৶৶ а§Єа•З ৙ৌ৪ а§Ж а§Ьৌ১а•З а§єа•Иа§Ва•§ ৙১ড়-৙১а•Н৮а•А а§Ха•З а§ђа•Аа§Ъ ৐৥৊১а•А ৶а•Ва§∞а§ња§ѓа•Ла§В а§Ха•Л а§Ха§Ѓ а§Ха§∞১ৌ а§єа•И, ৙а•Йа§°а•На§Є а§Ха•А а§Па§Ь а§Ѓа§ња§∞а•За§Ха§≤ а§Ха•На§∞а•Аа§Ѓ ১а•Л ৙ৌа§∞ড়৵ৌа§∞а§ња§Х а§∞ড়৴а•Н১а•Ла§В а§Ха•Л ৙а•На§∞а§Чৌ৥৊ а§Ха§∞১ৌ а§єа•И, а§Ха•Иа§°а§ђа§∞а•А а§Ха§Њ а§°а•За§ѓа§∞а•А а§Ѓа§ња§≤а•На§Х а§Ъа•Йа§Ха§≤а•За§Яа•§ а§ѓа§єа•А ৮৺а•Аа§В а§Ха§∞৵ৌ-а§Ъа•М৕, а§∞а§Ха•На§Ја§Њ-а§ђа§В৲৮, а§Фа§∞ ৵а•За§≤а•За§Ва§Яа§Ња§За§Ва§Є-а§°а•З а§Ха•Л ুৌ৮৮а•З а§Ха•З ৮ৌু ৙а§∞ а§≠а•А а§Ха§И ১а§∞а§є а§Ха•З ৵ড়а§Ьа•На§Юৌ৙৮ а§ђа§Ња§Ьа§Ња§∞ а§Ѓа•За§В а§Ж а§Ъа•Ба§Ха•З а§єа•Иа§Ва•§ ৵ড়а§Ьа•На§Юৌ৙৮а•Ла§В а§ХвАМа•А ৶а•Га§Ја•На§Яа§њ-৙а§∞а§ња§Іа§њ а§Єа•З а§Жа§Ь а§Ха•Ла§И а§≠а•А а§∞ড়৴а•Н১ৌ а§Еа§Ыа•В১ৌ ৮৺а•А а§єа•И, а§Ъа§Ња§єа•З ৵৺ ৙১ড়-৙১а•Н৮а•А, ৙а•На§∞а•За§Ѓа•А-৙а•На§∞а•За§Ѓа§ња§Ха§Њ а§Ха§Њ а§∞ড়৴а•Н১ৌ а§єа•Л, ুৌ১ৌ-৙ড়১ৌ а§Фа§∞ а§ђа§Ъа•На§Ъа•З а§Ха§Њ а§∞ড়৴а•Н১ৌ а§єа•Л а§ѓа§Њ а§Ђа§ња§∞ а§ђа•Йа§ЄвАН а§ѓа§Њ а§Ха•Ба§≤а•А а§Ха§Њ а§∞ড়৴а•Н১ৌ а§єа•Ла•§
ুৌ৮৵а•Аа§ѓ а§Єа§Ва§ђа§Ва§Іа•Ла§В а§Ха§Њ ৙а•Ва§∞а•А ১а§∞а§є а§Єа•З ৵а•Нৃ৵৪ৌৃа•Аа§Ха§∞а§£ а§Жа§Ь ৵ড়а§Ьа•На§Юৌ৙৮а•Ла§В а§Ѓа•За§В ৶ড়а§Ца§Ња§ѓа§Њ а§Ьৌ১ৌ а§єа•Иа•§ ৙а•Ва§∞а•З ৵ড়৴а•Н৵ а§Ѓа•За§В а§Єа•НвАН১а•На§∞а•А а§Фа§∞ ৙а•Ба§∞а•Ва§Ј а§Ха•З а§ђа•Аа§Ъ а§Єа§≠а•А а§Єа•Н১а§∞а•Ла§В ৙а§∞ а§єа•Л৮а•З ৵ৌа§≤а•З а§≠а•З৶а§≠ৌ৵ а§Ха•А а§Ъа§∞а•На§Ъа§Њ а§єа•Л а§∞а§єа•А а§єа•И, а§≤а•За§Хড়৮ а§єа§Ѓа§Ња§∞а•З ৵ড়а§Ьа•На§Юৌ৙৮ а§За§Є а§Ъа§∞а•На§Ъа§Њ а§Ха•Л ৙а•Ва§∞а•А ১а§∞а§є а§Єа•З а§Ца§Ња§∞а§ња§Ь а§Ха§∞১а•З а§єа•Иа§Ва•§ а§Жа§Ь ৵ড়а§Ьа•На§Юৌ৙৮а•Ла§В а§Ха•Л ৶а•За§Ц৮а•З а§Ха•З ৐ৌ৶ а§≤а§Ч১ৌ ৮৺а•Аа§В а§Ха§њ а§Єа•Ма§В৶а§∞а•На§ѓ а§Ха§Њ а§Ха•На§Ја•З১а•На§∞ а§Єа•Н১а•На§∞а§ња§ѓа•Ла§В а§Ха§Њ ৵ড়৴а•За§Ја§Ња§Іа§ња§Ха§Ња§∞ ৙а•На§∞ৌ৙а•Н১ а§Ха•На§Ја•З১а•На§∞ а§єа•Иа•§ а§Жа§Ь ৵ড়а§Ьа•На§Юৌ৙৮а•Ла§В а§Ѓа•За§В а§Ьа•Л ৙а•Ба§∞а•Ва§Ј а§Ж১ৌ а§єа•И, ৵৺ а§Ха•На§≤а•А৮-৴а•З৵а•На§° а§єа•Л১ৌ а§єа•И, ৵а•Иа§Ха•На§Є а§Ха§∞а§Ња§Ха•З, а§Ђа•З৴ড়ৃа§≤ а§Ха§∞а§Ња§Ха•З а§Фа§∞ а§Ца§Ња§Є а§Ѓа§∞а•Н৶а•Ла§В а§Ха•З а§≤а§ња§П а§Ж৮а•З ৵ৌа§≤а•А а§Ђа•За§ѓа§∞৮а•За§Є а§Фа§∞ ৪৮৪а•На§Ха•На§∞а•А৮ а§Ха•На§∞а•Аа§Ѓ а§Ха§Њ ৙а•На§∞а§ѓа•Ла§Ч а§Ха§∞а§Ха•З ৙а•Ва§∞а•А ১а§∞а§є а§Єа•З ১৕ৌа§Х৕ড়১ а§Ѓа•За§Яа•На§∞а•Ла§Єа•За§Ха•На§Єа•Ба§Еа§≤ а§Ѓа•И৮ а§Ха•А а§Ьа§ња§Є ১৪а•Н৵а•Аа§∞ а§Ха•Л ৙а•Ба§Ца•Н১ৌ а§Ха§∞১ৌ а§єа•И, а§Йа§Єа§Єа•З а§≤а§Ч১ৌ а§єа•И а§Ха§њ ৵৺ ৶ড়৮ ৶а•Ва§∞ ৮৺а•Аа§В а§Ьа§ђ ৙а•Ба§∞а•Ва§Ја•Ла§В а§Ха•З а§≤а§ња§П а§Ха§Ња§Ьа§≤ а§Фа§∞ а§≤ড়৙ড়৪а•На§Яа§ња§Х а§≠а•А а§ђа§Ња§Ьа§Ња§∞ а§Ѓа•За§В ৙а•З৴ а§Ха§ња§ѓа§Њ а§Ьа§Ња§Па§Ча§Ња•§ ৵а•Иа§Єа•З а§≠а•А а§Ха§И а§Ђа•И৴৮ ৴а•Ла§Ьа§Љ а§Ѓа•За§В ৙а•Ба§∞а•Ва§Ја•Л а§Ха•Л а§ђа§ња§В৶а•А а§≤а§Ча§Ња§П а§єа•Ба§П а§Єа•На§Ха§∞а•На§Я ৙৺৮а•З а§єа•Ба§П ৶ড়а§Ца§Ња§ѓа§Њ а§Ча§ѓа§Њ а§єа•Иа•§
৶а•Б৮ড়ৃৌ а§Ха•А а§Єа§≠а•А а§Єа§Ња§Ѓа§Ња§Ьа§ња§Х ৵а•Нৃ৵৪а•НвАН৕ৌа§Уа§В а§Ѓа•За§В а§Єа•НвАН১а•На§∞а•А ৺ৌ৴ড়а§П ৙а§∞ а§Ца§°а§Ља•А а§єа•Иа•§ ৺ৌ৴ড়а§П ৙а§∞ а§Ца§°а§Ља•А а§Єа•НвАН১а•На§∞а•А а§Ха•Л ৵ড়а§Ьа•На§Юৌ৙৮а•Ла§В а§Ха•З а§Ѓа§Ња§Іа•На§ѓа§Ѓ а§Єа•З а§Ђа§ња§∞ а§Єа•З ৙а§∞а§Ња§Іа•А৮১ৌ а§Ха•А а§ђа•За§°а§Ља§ња§ѓа§Ња§В ৙৺৮ৌа§И а§Ьа§Њ а§∞а§єа•А а§єа•Иа§Ва•§ ৵ড়а§Ьа•На§Юৌ৙৮а•Ла§В а§Ѓа•За§В а§Єа•НвАН১а•На§∞а•А а§Ха•З৵а§≤ ৵৪а•Н১а•Б а§ђа•За§Ъ৮а•З а§Ха§Њ ৪ৌ৲৮ ৐৮ а§Ха§∞ а§єа•А ৮৺а•Аа§В а§Ж১а•А а§єа•И, а§ђа§≤а•На§Ха§њ а§Єа•Н৵ৃа§В а§≠а•А а§Па§Х ৵৪а•Н১а•Б ৐৮ а§Ха§∞ а§єа•А ৙а•На§∞а§Єа•Н১а•Б১ а§єа•Л১а•А а§єа•Иа•§ а§Ьа§ња§Є ৙а§∞а§Ѓ а§Єа•Ба§В৶а§∞ а§Єа•НвАН১а•На§∞а•А а§Ха•А а§Ы৵ড় ৵ড়а§Ьа•На§Юৌ৙৮а•Ла§В а§Ха•З а§Ѓа§Ња§Іа•На§ѓа§Ѓ а§Єа•З ৪ৌু৮а•З а§Ж১а•А а§єа•И, а§Йа§Є а§Ы৵ড় а§Ха•Л ৵ৌ৪а•Н১৵ড়а§Х а§Ьа•А৵৮ а§Ѓа•За§В а§єа§Ња§Єа§ња§≤ а§Ха§∞৮ৌ а§≤а§Ча§≠а§Ч а§Еа§Єа§Ва§≠৵ а§єа•Иа•§ ৙৺а§≤а•А ৐ৌ১ ১а•Л а§ѓа§є а§єа•И а§Ха§њ а§Ѓа•Йа§°а§≤ а§Ха•А ৴ৌа§∞а•Аа§∞а§ња§Х ৐৮ৌ৵а§Я ৵ৌ৪а•Н১৵ড়а§Х а§Ьа•А৵৮ а§Ѓа•За§В ৙ৌа§Ва§Ъ а§Ђа•А৪৶а•А а§Єа•З а§Ьа•Нৃৌ৶ৌ а§Єа•Н১а•На§∞а§ња§ѓа•Ла§В а§Ха•З ৙ৌ৪ ৮৺а•Аа§В а§єа•Л১а•Аа•§ ৶а•Ва§Єа§∞а•А ৐ৌ১ а§ѓа§є а§єа•И а§Ха§њ а§Па§ѓа§∞-а§ђа•На§∞৴ড়а§Ва§Ч а§Фа§∞ а§Ђа•Ла§Яа•Л-৴а•Й৙ড়а§Ва§Ч а§Ьа•Иа§Єа•А ১а§Х৮а•Аа§Ха•Ла§В а§Ха§Њ а§За§Єа•Н১а•За§Ѓа§Ња§≤ а§Ха§∞а§Ха•З ১৪а•Н৵а•Аа§∞а•Ла§В а§Ѓа•За§В а§Ха§Ња§Ђа•А а§єа•За§∞-а§Ђа•За§∞ а§Ха§ња§ѓа§Њ а§Ьৌ১ৌ а§єа•Иа•§ а§За§Є ১а§∞а§є а§Ьа§ња§Є а§Е৙а•На§∞১ড়ু а§Єа•Ба§В৶а§∞১ৌ а§Ха§Њ ৙а•Иুৌ৮ৌ ৵ড়а§Ьа•На§Юৌ৙৮а•Ла§В а§Ха•З а§Ѓа§Ња§Іа•На§ѓа§Ѓ а§Єа•З ৪ৌু৮а•З а§Ж১ৌ а§єа•И а§Фа§∞ а§Ьа§ња§Єа•З ৶а•За§Ца§Ха§∞ ৵а•Иа§Єа§Њ ৐৮৮а•З а§Ха§Њ а§Еа§Єа§Ђа§≤ ৙а•На§∞а§ѓа§Ња§Є а§Ха§∞৮а•З ৵ৌа§≤а•А а§Ьа•Нৃৌ৶ৌ১а§∞ а§Єа•Н১а•На§∞а§ња§ѓа§Ња§В а§Ха•Ба§В৆ড়১ а§єа•Иа§В, ৵৺ а§Єа•Ба§В৶а§∞১ৌ а§Па§Х а§Ыа§≤ৌ৵а•З а§Ха•З ৪ড়৵ৌৃ а§Ха•Ба§Ы ৮৺а•Аа§Ва•§ а§За§Єа•А ১а§∞а§є, а§Па§Х ১а§∞а§Ђ ১а•Л а§єа§Ѓ ৙а•Ва§∞а•А ৶а•Б৮ড়ৃৌ а§Єа•З а§∞а§Ва§Ча§≠а•З৶ а§Фа§∞ ৮৪а•На§≤а§≠а•З৶ а§Ха•Л а§Ѓа§ња§Яৌ৮а•З а§Ха•А а§Ѓа§Ња§Ва§Ч а§Ха§∞ а§∞а§єа•З а§єа•Иа§В, а§≤а•За§Хড়৮ ৶а•Ва§Єа§∞а•А а§Уа§∞ ৵ড়а§Ьа•На§Юৌ৙৮а•Ла§В а§Ха•З а§Ѓа§Ња§Іа•На§ѓа§Ѓ а§Єа•З а§∞а§Ва§Ча§≠а•З৶ а§П৵а§В ৮৪а•На§≤а§≠а•З৶ а§Ха•Л ৐৥৊ৌ৵ৌ ৶а•З а§∞а§єа•З а§єа•Иа§Ва•§ ৵ড়а§Ьа•На§Юৌ৙৮а•Ла§В а§Ѓа•За§В а§Ж৮а•З ৵ৌа§≤а§Њ а§ѓа§є а§Єа•На§≤а•Ла§Ч৮ а§Ха§њ а§Ђа•За§ѓа§∞ а§≤৵а§≤а•А а§єа•А а§єа•Л১ৌ а§єа•И, а§Ха§ња§Єа•А а§≠а•А а§Хু১а§∞ а§∞а§Ва§Ч а§Ха•А а§Єа•НвАН১а•На§∞а•А а§Фа§∞ ৙а•Ба§∞а•Ва§Ј а§Ха•Л а§єа•А৮а§≠ৌ৵৮ৌ а§Єа•З а§≠а§∞ ৶а•З৮а•З а§Ха•З а§≤а§ња§П а§Ха§Ња§Ђа•А а§єа•Л১ৌ а§єа•Иа•§ ১а•Н৵а§Ъа§Њ а§Ха•З а§Ча•Ла§∞а•З а§∞а§Ва§Ч а§Ха•Л а§Ха§Ња§≤а•З а§∞а§Ва§Ч а§Ха•З а§К৙а§∞ ৙а•На§∞ৌ৕ুড়а§Х১ৌ ৶а•З৮ৌ, ৪ুৌ৮১ৌ а§Ха•З а§єа§Ѓа§Ња§∞а•З а§Єа§В৵а•И৲ৌ৮ড়а§Х ৶ৌ৵а•З а§Ха•Л а§≠а•А а§Эа•Ва§В৆ৌ ৪ৌ৐ড়১ а§Ха§∞১ৌ а§єа•Иа•§ а§Ха•Ба§Ы а§єа•А а§Єа§Ѓа§ѓ ৙৺а§≤а•З а§Па§Х а§Ѓа•Иа§Ча•На§Ьа•А৮ а§Ха•З а§Х৵а§∞ ৙а•Га§Ја•Н৆ ৙а§∞ а§Р৴а•Н৵а§∞а•На§ѓа§Њ а§∞а§Ња§ѓ а§Ха•А а§Ьа•Л ১৪а•Н৵а•Аа§∞ а§Жа§Иа§В ৕а•А, ৵৺ а§≠а•А ৵ড়৵ৌ৶ а§Ха§Њ а§Ха§Ња§∞а§£ ৐৮а•А ৕а•А, а§Ха•На§ѓа•Ла§Ва§Ха§њ а§Йа§Єа§Ѓа•За§В а§Р৴а•Н৵а§∞а•На§ѓа§Њ а§Ха•А ১а•Н৵а§Ъа§Њ а§Ха•З а§∞а§Ва§Ч а§Ха•Л а§Фа§∞ а§єа§≤а•На§Ха§Њ а§Ха§ња§ѓа§Њ а§Ча§ѓа§Њ а§•а§Ња•§ а§Ьа§Ња§єа§ња§∞ а§Єа•А ৐ৌ১ а§єа•И а§Ха§њ ৵ড়৴а•Н৵ а§Ха•З а§Ха§И а§Єа§Ѓа•Б৶ৌৃ а§Ха•З а§≤а•Ла§Ч а§Ьа•Иа§Єа•З а§Еа§Ђа•На§∞а•Аа§Ха•А-а§Еа§Ѓа•За§∞а§ња§Ха§Њ а§Єа§Ѓа•Б৶ৌৃ а§ѓа§Њ а§≠а§Ња§∞১ а§Ѓа•За§В а§єа•А ৶а•На§∞৵ড়ৰ৊ а§Фа§∞ а§Ж৶ড়৵ৌ৪а•А а§Єа§Ѓа•Б৶ৌৃ а§Ха•З а§≤а•Ла§Ч, а§Ьড়৮а§Ха•А ১а•Н৵а§Ъа§Њ а§Ха§Њ а§∞а§Ва§Ч а§Ча§єа§∞а§Њ а§єа•Л১ৌ а§єа•И, ৵а•З а§За§Є ৙а•На§∞а§Ха§Ња§∞ а§Ха•З ৵ড়а§Ьа•На§Юৌ৙৮а•Ла§В а§Єа•З ৮ а§Єа§ња§∞а•На§Ђ а§Єа•Н৵ৃа§В а§Ха•Л а§Е৙ুৌ৮ড়১ а§Ѓа§єа§Єа•Ва§Є а§Ха§∞а•За§Ва§Ча•З, а§ђа§≤а•На§Ха§њ а§Ха•Ба§В৆ড়১ а§≠а•А а§єа•Ла§Ва§Ча•За•§
а§Єа•НвАН১а•На§∞а•А-а§Ѓа•Ба§Ха•Н১ড় а§Ха•З ৮ৌু ৙а§∞ а§Ьа§ња§Є ১а§∞а§є а§Єа•З ৵ড়а§Ьа•На§Юৌ৙৮а•Ла§В а§Ха•Л ৙а•На§∞а§Єа•Н১а•Б১ а§Ха§ња§ѓа§Њ а§Ьа§Њ а§∞а§єа§Њ а§єа•И, а§Йа§Єа§Єа•З а§Єа•НвАН১а•На§∞а•А-а§Ѓа•Ба§Ха•Н১ а§єа•Л৮а•З а§Ха•А а§ђа§Ьа§Ња§ѓ а§Ђа§ња§∞ а§Єа•З ৙а§∞а§Ња§Іа•А৮ а§єа•Л а§∞а§єа•А а§єа•Иа•§ а§Еа§Ча§∞ ৙а•Ба§∞ৌ৮а•З ৶а•Ма§∞ а§Ѓа•За§В а§Єа•НвАН১а•На§∞а•А ৙ড়১а•Г৪১а•Н১ৌ১а•На§Ѓа§Х а§Єа§Ња§Ѓа§Ња§Ьа§ња§Х ৵а•Нৃ৵৪а•НвАН৕ৌ а§Ха•А ৶ৌ৪ ৕а•А ১а•Л а§Жа§Ь а§Й৙а§≠а•Ла§Ха•Н১ৌ৵ৌ৶а•А а§Єа§Ва§Єа•На§Ха•Г১ড় а§Ха•Аа•§ ৶а•За§є а§Єа•З а§Ѓа•Ба§Ха•Н১ড় а§Ха•З ৮ৌু ৙а§∞ а§Йа§Єа§Ха§Њ ৵ড়а§Ьа•На§Юৌ৙৮а•Ла§В а§Ха•З а§Ѓа§Ња§Іа•На§ѓа§Ѓ а§Єа•З а§ђа§Ња§Ьа§Ња§∞а•Аа§Ха§∞а§£ а§єа•Л а§∞а§єа§Њ а§єа•Иа•§ ৵ড়а§Ьа•На§Юৌ৙৮ ৮ড়а§∞а•Нুৌ১ৌ а§ѓа§є а§Ьৌ৮১а•З а§єа•Иа§В а§Ха§њ а§ђа§Ъа•На§Ъа•Ла§В а§Ха•З а§Ха•Ла§Ѓа§≤ а§Ѓа§Єа•Н১ড়ৣа•На§Х ৙а§∞ ৵ড়а§Ьа•На§Юৌ৙৮а•Ла§В а§Ха§Њ а§Ча§єа§∞а§Њ а§Еа§Єа§∞ ৙ৰ৊১ৌ а§єа•И, а§За§Єа§≤а§ња§П а§Й৮а§Ха§Њ ৙а•На§∞а§ѓа§Ња§Є а§ѓа§є а§∞৺১ৌ а§єа•И а§Ха§њ а§Єа§ђа§Єа•З а§Ьа•Нৃৌ৶ৌ а§ђа§Ъа•На§Ъа•Ла§В а§Ха•Л ৙а•На§∞а§≠ৌ৵ড়১ а§Ха§ња§ѓа§Њ а§Ьа§Ња§Па•§ а§ђа§Ъа•На§Ъа•Ла§В а§Ха•З а§Ха§Ња§∞а•На§Яа•В৮ а§Іа§Ња§∞ৌ৵ৌ৺ড়а§Ха•Ла§В а§Ѓа•З а§Ж৮а•З ৵ৌа§≤а•З а§≤а•Ла§Х৙а•На§∞а§ња§ѓ ৙ৌ১а•На§∞ а§Ьа•Иа§Єа•З а§°а•Ла§∞а•За§Ѓа•Й৮, а§Ыа•Ла§Яа§Њ а§≠а•Аа§Ѓ ৵а§Ча•Иа§∞а§є а§Ха•Л а§≠а•А ৵ড়а§Ьа•На§Юৌ৙৮а•Ла§В а§Ѓа•За§В ৙а•На§∞а§Єа•Н১а•Б১ а§Ха§ња§ѓа§Њ а§Ьа§Њ а§∞а§єа§Њ а§єа•Иа•§ а§Ьа§Ња§єа§ња§∞ а§Єа•А ৐ৌ১ а§єа•И а§Ха§њ а§ђа§Ъа•На§Ъа•З а§Е৙৮а•З ৙а•На§∞а§ња§ѓ ৙ৌ১а•На§∞а•Ла§В а§Ха•Л а§Ьа•Л а§Ха•Ба§Ы а§≠а•А а§Цৌ১а•З-৙а•А১а•З а§ѓа§Њ ৙৺৮а•З а§єа•Ба§П ৶а•За§Ца•За§Ва§Ча•З, а§Йа§Єа•З а§єа•А а§Е৙৮а•З а§Еа§≠а§ња§≠ৌ৵а§Ха•Ла§В а§Єа•З а§Ца§∞а•А৶৮а•З а§Ха•А а§Ь৊ড়৶ а§Ха§∞а•За§Ва§Ча•За•§ а§ђа§Ъа•На§Ъа•Ла§В а§Ха•Л ৮ৌа§∞а§Ња§Ьа§Љ а§Ха§∞৮ৌ а§Ж৪ৌ৮ ৮৺а•Аа§В, а§За§Єа§≤а§ња§П ুৌ১ৌ-৙ড়১ৌ а§≠а•А а§ђа§Ъа•На§Ъа•Ла§В а§Ха•А а§Ь৊ড়৶ ৙а•Ва§∞а•А а§Ха§∞а•За§Ва§Ча•З а§єа•А а§Фа§∞ а§За§Є ১а§∞а§є ৮ а§Єа§ња§∞а•На§Ђ а§ђа§Ъа•На§Ъа•З, а§ђа§≤а•На§Ха§њ а§Па§Х ৙а•Ва§∞а§Њ ৙а§∞ড়৵ৌа§∞ а§єа•А ৵ড়а§Ьа•На§Юৌ৙৮а•Ла§В а§Ха§Њ ৴ড়а§Ха§Ња§∞ ৐৮ а§Ьৌ১ৌ а§єа•Иа•§ а§ђа§Ъа•На§Ъа•Ла§В а§Ха•А а§≤а•Ла§Х৙а•На§∞а§ња§ѓ а§°а•Йа§≤ а§єа•И, а§ђа§Ња§∞а•На§ђа•А а§°а•Йа§≤ а§Ьа§ња§Єа•З а§ђа§Ъа•На§Ъа•З а§Е৙৮ৌ а§Єа•На§Яа•За§Яа§Є а§Єа§ња§Ва§ђа§≤ ুৌ৮১а•З а§єа•Иа§Ва•§ а§ђа§Ња§∞а•На§ђа•А а§Ха•З ৮ а§Ьৌ৮а•З а§Хড়১৮а•З а§Єа§Ва§Єа•На§Ха§∞а§£ а§ђа§Ња§Ьа§Ња§∞ а§Ѓа•За§В а§Ѓа•Ма§Ьа•В৶ а§єа•Иа§Ва•§ а§ѓа§єа•А ৮৺а•Аа§В, а§ђа§Ња§∞а•На§ђа•А а§Ха•З а§єа•За§ѓа§∞ а§Ха•Л а§Ха§≤а§∞ а§Фа§∞ ৴а•Иа§В৙а•В а§Ха§∞৮а•З а§Ха•З а§≤а§ња§П а§Й১а•Н৙ৌ৶ а§≠а•А а§ђа§Ња§Ьа§Ња§∞ а§Ѓа•За§В а§Ж а§Ъа•Ба§Ха•З а§єа•Иа§Ва•§ а§ђа§Ња§∞а•На§ђа•А а§°а•Йа§≤ а§Ха•А а§За§Єа•А а§≤а•Ла§Х৙а•На§∞ড়ৃ১ৌ а§Ха•Л а§≠а•Б৮ৌ৮а•З а§Ха•З а§≤а§ња§П ৙а•Й৙ а§Ча•На§∞а•Б৙ а§Ра§Ха•Н৵ৌ ৮а•З 1997 а§Ѓа•За§В а§Жа§За§Па§Ѓ а§П а§ђа§Ња§∞а•На§ђа•А а§Чৌ৮ৌ а§∞а§ња§≤а•Аа§Ь а§Ха§ња§ѓа§Њ ৕ৌ, а§Ьа•Л а§Ха§њ а§Ѓа•Иа§Яа§≤ а§Єа•З а§Й১а•Н৙ৌ৶ড়১ а§ђа§Ња§∞а•На§ђа•А а§Фа§∞ а§Ха•З৮ а§°а•Йа§≤а•На§Є а§Ха•З ৵ড়ৣৃ а§Ѓа•За§В а§єа•И, а§ѓа§єа•А ৮৺а•Аа§В а§Чৌ৮а•З а§Ѓа•За§В а§ђа§Ња§∞а•На§ђа•А а§Ха•З а§≤а§ња§П а§ђа•На§≤а•Йа§°а•А а§Фа§∞ а§ђа§ња§Ва§ђа•Л а§Ьа•Иа§Єа•З ৵ড়৴а•За§Ја§£а•Ла§В а§Ха§Њ ৙а•На§∞а§ѓа•Ла§Ч а§Ха§ња§ѓа§Њ а§Ча§ѓа§Њ а§єа•И, а§Ьа•Л а§Йа§Є а§Єа•НвАН১а•На§∞а•А а§Ха•Л ৙а•На§∞а§Єа•Н১а•Б১ а§Ха§∞১а•З а§єа•Иа§В, а§Ьа•Л а§Ха§њ ৴ৌа§∞а•Аа§∞а§ња§Х а§∞а•В৙ а§Єа•З а§Єа•Ба§В৶а§∞ ১а•Л а§єа•И, ৙а§∞а§В১а•Б ৶ড়ুৌа§Ч а§Єа•З а§Хু১а§∞ а§єа•Иа§Ва•§ а§Па§Ха•Н৵ৌ а§Ха•А а§ѓа§є а§ђа§Ња§∞а•На§ђа•А а§Е৙৮а•З а§Ша•Ба§Я৮а•Ла§В ৙а§∞ а§Эа•Ба§Ха•А а§єа•Ба§И а§єа•И а§Фа§∞ а§Е৙৮а•З ৙а•На§∞а•За§Ѓа•А а§Ха•Л а§Ца•Б৴ а§Ха§∞৮а•З а§Ха•З а§≤а§ња§П а§Ха•Ба§Ы а§≠а•А а§Ха§∞৮а•З а§Ха•Л ১а•Иа§ѓа§Ња§∞ а§єа•Иа•§ а§Ѓа•Иа§Яа§≤ а§Ха§В৙৮а•А а§Ха•З а§Ж৙১а•Н১ড় а§Ь১ৌ৮а•З а§Ха•З ৐ৌ৵а§Ьа•В৶ а§≠а•А а§За§Є а§Чৌ৮а•З а§Ха•Л ৙а•На§∞১ড়৐а§В৲ড়১ ৮৺а•Аа§В а§Ха§ња§ѓа§Њ а§Ьа§Њ а§Єа§Ха§Ња•§ а§За§Є а§Чৌ৮а•З а§Ѓа•За§В а§Єа•НвАН১а•На§∞а•А а§Ха•А а§Ьа•Л а§Ы৵ড় а§Йа§≠а§∞ а§Ха§∞ ৪ৌু৮а•З а§Ж১а•А а§Ж১а•А а§єа•И, ৵৺ а§Ыа•Ла§Яа•А а§ђа§Ъа•На§Ъа§ња§ѓа•Ла§В а§Ха•Л ৙а•Ба§∞а•Ва§Ј а§Ха•З а§Еа§Іа•А৮৪а•НвАН৕ ৐৮а•З а§∞৺৮а•З а§Ха•З а§≤а§ња§П ুৌ৮৪ড়а§Х а§∞а•В৙ а§Єа•З ১а•Иа§ѓа§Ња§∞ а§Ха§∞৮а•З а§Ха•З а§≤а§ња§П а§Ха§Ња§Ђа•А а§єа•Иа•§ а§ѓа§є а§Ж৴а•На§Ъа§∞а•На§ѓа§Ь৮а§Х ৮৺а•Аа§В а§єа•И а§Ха§њ а§За§Є а§Чৌ৮а•З а§Ха•А а§Ж৆ а§Еа§∞а§ђ ৙а•На§∞১ড়ৃৌа§В а§ђа§ња§Х а§Ъа•Ба§Ха•А а§єа•Иа§Ва•§
а§≤а•Ла§Х৙а•На§∞а§ња§ѓ а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓа•А а§єа§Єа•Н১ড়ৃৌа§В а§Фа§∞ а§Ца§ња§≤а§Ња§°а§Ља•А ৵ড়а§≠ড়৮а•Н৮ а§ђа•На§∞а§Ња§Ва§°а•На§Є а§Ха§Њ а§Па§Ва§ђа•За§Єа§°а§∞ ৐৮ а§Ха§∞ а§Ж а§∞а§єа•З а§єа•Иа§Ва•§ а§Ха§ња§Єа•А а§Ца§Ња§Є а§Й১а•Н৙ৌ৶ а§Ха•Л ৙а•На§∞а§ѓа•Ба§Ха•Н১ а§Ха§∞৮а•З а§Ха•З а§≤а§ња§П ৵а•З а§Й৙а§≠а•Ла§Ха•Н১ৌ-৶а§∞а•Н৴а§Х ৵ৌ৪а•Н১৵ড়а§Х а§Еুড়১ৌа§≠ а§ђа§Ъа•На§Ъ৮ а§ѓа§Њ ৵ৌ৪а•Н১৵ড়а§Х а§Єа§Ъড়৮ ১а•За§В৶а•Ба§≤а§Ха§∞ а§Ха•Л ৮৺а•Аа§В а§Ьа§Ња§®а§§а§Ња•§ ৵৺ а§Єа§ња§∞а•На§Ђ а§Й৮а§Ха•А а§Йа§Є а§Єа•Б৙а§∞-а§За§Ѓа•За§Ь а§Ха•Л а§Ьৌ৮১ৌ а§єа•И, а§Ьа•Л ৵ড়а§Ьа•На§Юৌ৙৮а•Ла§В а§Ха•З а§Ѓа§Ња§Іа•На§ѓа§Ѓ а§Єа•З ৪ৌু৮а•З а§Ж১а•А а§єа•Иа•§ а§За§Є ৙а•На§∞а§Ха§Ња§∞ а§Й৙а§≠а•Ла§Ха•Н১ৌ, ৵ৌ৪а•Н১৵ড়а§Х১ৌ а§Ха•Л а§≠а•А а§Ы৵ড়ৃа•Ла§В а§Ѓа•За§В ৶а•За§Ц১ৌ а§єа•Иа•§ а§За§Іа§∞ ৵ড়а§Ьа•На§Юৌ৙৮-а§Ха§В৙৮ড়ৃৌа§В-а§Па§Ьа•За§Ва§Єа§ња§ѓа§Ња§В а§≠а•А а§Ъа§Ња§≤а§Ња§Х а§єа•Л а§Ча§И а§єа•Иа§Ва•§ а§Й৮а•На§єа•За§В а§ѓа§є ৙১ৌ а§Ъа§≤ а§Ъа•Ба§Ха§Њ а§єа•И а§Ха§њ а§Жа§Ь а§Ха§Њ а§Й৙а§≠а•Ла§Ха•Н১ৌ а§Ха§ња§Єа•А а§≠а•А ৙а•За§Ь-৕а•На§∞а•А а§Єа•За§≤а§ња§ђа•На§∞а§ња§Яа•А а§Ха•З а§Йа§Є ৶ৌ৵а•З ৙а§∞ а§Жа§Ва§Ц а§Ѓа•Ва§В৶ а§Ха§∞ ৵ড়৴а•Н৵ৌ৪ ৮৺а•Аа§В а§Ха§∞১ৌ,а§Ьа•Л ৵৺ а§Ха§ња§Єа•А а§Й১а•Н৙ৌ৶৮ а§Ха•З ৵ড়а§Ьа•На§Юৌ৙৮ а§Ѓа•За§В а§Ха§∞১а•З а§єа•Иа§В, а§За§Єа§≤а§ња§П ৵ড়а§Ьа•На§Юৌ৙৮ а§Ха§Њ а§Па§Х ৮ৃৌ а§Ьа§∞а§ња§ѓа§Њ ৮ড়а§Ха§Ња§≤а§Њ а§Ча§ѓа§Њ а§єа•И а§Фа§∞ ৵৺ а§єа•И-а§Е৙а•На§∞১а•На§ѓа§Ха•На§Ј а§∞а•В৙ а§Єа•З ৵ড়а§Ьа•На§Юৌ৙৮ а§Ха•А ৙а•На§∞а§Єа•Н১а•Ба§§а§ња•§ а§Еа§Ча§∞ а§≤а•Ла§Ча•Ла§В а§Ха•А ৃৌ৶৶ৌ৴а•Н১ а§Еа§≠а•А а§Іа•Ба§Ва§Іа§≤а•А ৮৺а•Аа§В а§єа•Ба§И а§єа•Л ১а•Л 1997 а§Ѓа•За§В ৙а•На§∞৶а§∞а•Н৴ড়১ а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓ а§єа§ња§Ѓа§Ња§≤а§ѓ ৙а•Б১а•На§∞ а§Ха§Њ а§Ьа§ња§Ха•На§∞ а§Ха§ња§ѓа§Њ а§Ьа§Њ а§Єа§Х১ৌ а§єа•Иа•§ а§За§Є а§Ђа§ња§≤а•На§Ѓ а§Ѓа•За§В а§єа•Аа§∞а•Л а§Еа§Ха•На§Ја§ѓ а§Ц৮а•Н৮ৌ а§Ха•Л а§Ча•Л৶а§∞а•За§Ь а§Ха•З а§Єа§ња§В৕а•Йа§≤ а§Єа§Ња§ђа•Б৮ а§Єа•З ৮৺ৌ১а•З а§єа•Ба§П ৶ড়а§Ца§Ња§ѓа§Њ а§Ча§ѓа§Њ а§•а§Ња•§ а§За§Єа•А ৙а•На§∞а§Ха§Ња§∞ а§Жа§Ьа§Ха§≤ ৵ড়а§≠ড়৮а•Н৮ ৙а•На§∞а§Ха§Ња§∞ а§Ха•З а§Єа•Н৙а•Ла§∞а•На§Яа•На§Є а§ѓа§Њ а§Ъа•Иа§∞а§ња§Яа•А а§З৵а•За§Ва§Яа•На§Є а§Фа§∞ а§Ђа•И৴৮ ৴а•Ла§Ьа§Љ а§Ха•З ৶а•Ма§∞ৌ৮ ৙а•За§Ь-৕а•На§∞а•А а§Єа•За§≤а§ња§ђа•На§∞а§ња§Яа•Аа§Ьа§Љ а§Ха•Л ৵ড়а§≠ড়৮а•Н৮ а§Ха§В৙৮ড়ৃа•Ла§В а§Ха•З а§Й১а•Н৙ৌ৶ а§Іа§Ња§∞а§£ а§Ха§ња§П а§єа•Ба§П ৶а•За§Ца§Њ а§Ьа§Њ а§Єа§Х১ৌ а§єа•Иа•§ ৶а§∞а•Н৴а§Ха•Ла§В ৙а§∞ а§Е৙৮а•А а§Ча§ња§∞а§Ђа•Н১ а§Ѓа§Ьа§ђа•В১ а§Ха§∞৮а•З а§Ха•З а§≤а§ња§П а§ѓа§Њ а§Е৙৮а•А ৵ড়৴а•Н৵৪৮а•Аৃ১ৌ ৐৥ৌ৊৮а•З а§Ха•З а§≤а§ња§П а§≤а•А а§Й১а•Н৙ৌ৶а§Х а§За§Є ১а§∞а§є а§Єа•З а§Е৙а•На§∞১а•На§ѓа§Ха•На§Ј ৵ড়а§Ьа•На§Юৌ৙৮а•Ла§В а§Ха§Њ ৙а•На§∞а§ѓа•Ла§Ч а§Ха§∞ а§∞а§єа•З а§єа•Иа§Ва•§ ৵ড়а§Ьа•На§Юৌ৙৮а•Ла§В а§Ха•А а§Й৙৪а•Н৕ড়১ড় а§Жа§Ь а§Єа§∞а•Н৵৵а•Нৃৌ৙а•А а§єа•Иа•§ а§Й৮৪а•З а§ђа§Ъ৮ৌ а§≤а§Ча§≠а§Ч а§Еа§Єа§Ва§≠৵ а§єа•Иа•§ а§Жа§Ь а§Ъа§Ња§єа•З ৙১а•На§∞-৙১а•На§∞а§ња§Ха§Ња§Па§В а§єа•Ла§В, а§Яа•А৵а•А а§ѓа§Њ а§Ха§В৙а•На§ѓа•Ва§Яа§∞ а§єа•Л, а§Ѓа•Ла§ђа§Ња§За§≤ а§Ђа•Л৮ а§єа•Л, ৙а•За§Яа•На§∞а•Ла§≤ ৙а§В৙ а§єа•Ла§В, а§Ъа•Ма§∞а§Ња§єа•З ৙а§∞ а§≤а§Ча•З ৙а•Ла§Єа•На§Яа§∞ а§єа•Ла§В, а§Ха•Ла§И а§Єа§Ња§∞а•Н৵а§Ь৮ড়а§Х а§Ха§Ња§∞а•На§ѓа§Ха•На§∞а§Ѓ а§єа•Л, ৵ড়а§Ьа•На§Юৌ৙৮ а§єа§∞ а§Ьа§Ча§є а§Ѓа•Ма§Ьа•В৶ а§єа•Иа§Ва•§
а§єа§Ѓа§Ња§∞а•А а§Єа§В৙а•Ва§∞а•На§£ а§Ьа•А৵৮-৴а•Иа§≤а•А а§єа•А ৵ড়а§Ьа•На§Юৌ৙৮а•Ла§В а§Єа•З ৮ড়а§∞а•Н৶а•З৴ড়১ а§Фа§∞ ৮ড়а§∞а•На§Іа§Ња§∞ড়১ а§єа•Л а§∞а§єа•А а§єа•Иа•§ ৵ড়а§Ьа•На§Юৌ৙৮а•Ла§В а§Ха•З а§Жа§Ха§∞а•На§Ја§Х а§Ѓа§Ња§ѓа§Њ-а§Ьа§Ња§≤ а§Ѓа•За§В а§Ђа§Ва§Єа•З ৶а§∞а•Н৴а§Х а§Ха•Л а§ѓа§є ৙১ৌ а§єа•А ৮৺а•Аа§В а§Ъа§≤ ৙ৌ১ৌ а§Ха§њ ৵৺ ৵ৌ৪а•Н১৵ а§Ѓа•За§В ৙а•На§∞а§Ња§ѓа•Ла§Ьа§Ха•Ла§В а§Ха•З ৺ৌ৕а•Ла§В а§ђа•За§Ъа§Њ а§Ьа§Њ а§Ъа•Ба§Ха§Њ а§єа•И а§Фа§∞ а§Йа§Єа§Ха•А а§Єа•Ла§Ъ ৙а§∞ а§≠а•А ৵ড়а§Ьа•На§Юৌ৙৮а•Ла§В а§Ха§Њ а§єа•А ৮ড়ৃа§В১а•На§∞а§£ а§єа•Иа•§ а§За§Є а§Й১а•Н৙ৌ৶а•Ла§В а§Ха•Л ৙а•На§∞а§ѓа•Ба§Ха•Н১ а§Ха§∞১а•З-а§Ха§∞১а•З ৵৺ а§Єа•Н৵ৃа§В а§≠а•А а§Па§Х ৵৪а•Н১а•Б а§Ѓа•За§В ১৐а•Н৶а•Аа§≤ а§єа•Л а§Ьৌ১ৌ а§єа•Иа•§ а§Жа§Ь ৵ড়а§Ьа•На§Юৌ৙৮а•Ла§В а§Ха§Њ а§Ђа•Иа§≤ৌ৵ ৐৥৊১ৌ а§єа•А а§Ьа§Њ а§∞а§єа§Њ а§єа•Иа•§ а§Па§Х а§Ф৪১ а§Еа§Ѓа•За§∞а§ња§Ха•А а§Ха•Л а§Ха§∞а•Аа§ђ ৙а§В৶а•На§∞а§є а§Єа•М ৵ড়а§Ьа•На§Юৌ৙৮ ৙а•На§∞১ড়৶ড়৮ ৶а•За§Ц৮а•З ৙ৰ৊১а•З а§єа•Иа§Ва•§ а§ѓа§єа•А ৮৺а•Аа§В, а§Еа§Ѓа•За§∞а§ња§Ха§Њ а§Ѓа•За§В а§єа§∞ а§Єа§Ња§≤ а§≤а§Ча§≠а§Ч а§Ж৆ а§Еа§∞а§ђ а§°а•Йа§≤а§∞ ৵ড়а§Ьа•На§Юৌ৙৮а•Ла§В а§Ха§Њ а§Ца§∞а•На§Ъ а§Ха§ња§П а§Ьৌ১а•З а§єа•Иа§Ва•§ а§ђа§єа•Ба§∞а§Ња§Ја•На§Яа•На§∞а•Аа§ѓ а§Ха§В৙৮ড়ৃৌа§В, ৵ড়а§Ьа•На§Юৌ৙৮а•Л а§Ха•А ু৶৶ а§Єа•З ৮ а§Єа§ња§∞а•На§Ђ ৵а•И৴а•Н৵ড়а§Х а§Фа§∞ а§Єа•НвАН৕ৌ৮а•Аа§ѓ а§Ы৵ড়ৃа•Ла§В а§Ха§Њ ৮ড়а§∞а•На§Ѓа§Ња§£ а§Ха§∞ а§∞а§єа•А а§єа•Иа§В, а§ђа§≤а•На§Ха§њ а§Й৮а§Ха§Њ ৙а•На§∞а§Ъа§Ња§∞ а§Фа§∞ ৙а•На§∞а§Єа§Ња§∞ а§≠а•А а§Ха§∞ а§∞а§єа•А а§єа•Иа§Ва•§ а§Єа§Ња§Ѓа•Ва§єа§ња§Х১ৌ а§Ха•З а§Єа•НвАН৕ৌ৮ ৙а§∞ а§Жа§Ь ৵ড়а§Ьа•На§Юৌ৙৮а•Ла§В а§Ха•З а§Ѓа§Ња§Іа•На§ѓа§Ѓ а§Єа•З ৵а•Иа§ѓа§Ха•Н১ড়১ৌ а§Ха•Л ৐৥৊ৌ৵ৌ ৶ড়ৃৌ а§Ьа§Њ а§∞а§єа§Њ а§єа•Иа•§ а§За§Ха•На§Ха•А৪৵а•Аа§В ৪৶а•А а§Ѓа•За§В ৵ড়а§Ха§Ња§Є а§Ха•А ৙а§∞а§ња§≠а§Ња§Ја§Њ а§Ха•З৵а§≤ а§Єа§Ха§≤ а§∞а§Ња§Ја•На§Яа•На§∞а•Аа§ѓ а§Й১а•Н৙ৌ৶ а§Фа§∞ а§Жа§ѓ а§Ха•З ুৌ৮а§Ха•Ла§В ১а§Х а§єа•А а§Єа§ња§Ѓа§Я а§Ха§∞ а§∞а§є а§Ча§И а§єа•Иа•§ ৵ড়а§Ха§Ња§Є а§Ха•А а§За§Є ৙а§∞а§ња§≠а§Ња§Ја§Њ ৮а•З ুৌ৮৵ а§Ха•З а§Й১а•Н৙ৌ৶а§Х а§Фа§∞ а§Йа§≠а•Ла§Ха•Н১ৌ а§Єа•Н৵а§∞а•В৙ а§Ха•А ৙а§∞а§ња§Ха§≤а•Н৙৮ৌ а§Ха•Л а§єа•А ৶а•Г৥৊ а§Ха§ња§ѓа§Њ а§єа•Иа•§ ৵ড়а§Ьа•На§Юৌ৙৮ а§Жа§Ь а§Й৙а§≠а•Ла§Ха•Н১ৌ৵ৌ৶а•А а§Єа§Ва§Єа•На§Ха•Г১ড় а§Ха•Л ৐৥৊ৌ৵ৌ ৶а•З৮а•З а§Ха•Л а§єа§∞ а§Єа§Ва§≠৵ ৙а•На§∞а§ѓа§Ња§Є а§Ха§∞ а§∞а§єа•З а§єа•Иа§Ва•§ а§Ђа•На§∞а§Ња§Ва§Єа•Аа§Єа•А ৵ড়а§Ъа§Ња§∞а§Х а§Ьа§ѓа§Њ а§ђа•Й৶а•На§∞а•Аа§≤а§Њ а§Ха•З а§Ѓа•Б১ৌ৐ড়а§Х а§Й৙а§≠а•Ла§Ха•Н১ৌ৵ৌ৶а•А а§Єа§Ва§Єа•На§Ха•Г১ড় ৮а•З ু৮а•Ба§Ја•На§ѓ а§Ха•А а§Ьа§∞а•Ва§∞১ а§Фа§∞ а§Й১а•Н৙ৌ৶а§Х১ৌ а§Ха•З а§Ѓа§Іа•На§ѓ ৮а§Ха§Ња§∞ৌ১а•На§Ѓа§Х а§Єа§Ва§ђа§Ва§І ৐৮ৌৃৌ а§єа•И, а§Й৙а§≠а•Ла§Ха•Н১ৌ৵ৌ৶ а§Ѓа•За§В а§Єа§Ѓа§Ња§Ь а§Па§Х а§єа§ња§Єа•На§Яа•Аа§∞а§ња§ѓа§Њ а§Ха•А а§Е৵৪а•НвАН৕ৌ а§Ѓа•За§В ৙৺а•Ба§Ва§Ъ а§Ьৌ১ৌ а§єа•И, а§Ьа§ња§Єа§Ха§Њ ৪ড়৶а•На§Іа§Ња§В১ а§єа•И а§Еа§Іа§ња§Х а§Фа§∞ а§Еа§Іа§ња§Х, а§Ха§≠а•А а§≠а•А ৃ৕а•За§Ја•На§Я ৮৺а•Аа§Ва•§ а§За§Є ৙а•На§∞а§Ха§Ња§∞ а§Єа•Ба§Ц-а§Єа§Ва§Ъа§ѓ а§Ха•А а§≤а§Ња§≤а§Єа§Њ а§єа•А а§Й৙а§≠а•Ла§Ч а§Ха•А ৙а•На§∞а§Ха•На§∞а§ња§ѓа§Њ а§Ха•Л а§Ьа§∞а•Ва§∞১ а§Єа•З а§Ьа•Нৃৌ৶ৌ ৮ড়ৃа§В১а•На§∞ড়১ а§Ха§∞১а•А а§єа•Иа•§ ৵ড়а§Х৪ড়১ ৶а•З৴а•Ла§В а§Ѓа•За§В а§Х৙ৰ৊а•З, а§Ђа§∞а•Н৮а•Аа§Ъа§∞ а§Фа§∞ а§ѓа§єа§Ња§В ১а§Х а§Ха§њ а§Ча§Ња§°а§Ља•А а§Ьа•Иа§Єа•А ৵৪а•Н১а•Ба§Па§В а§≠а•А а§≠а•М১ড়а§Х а§∞а•В৙ а§Єа•З а§Ьа•Аа§∞а•На§£-а§Ха•На§Ја•Аа§∞а•На§£ а§єа•Л৮а•З а§Єа•З ৙৺а§≤а•З а§єа•А ু৮а•Ба§Ја•На§ѓ ৆ড়а§Хৌ৮а•З а§≤а§Ча§Њ ৶а•З১ৌ а§єа•И, а§Ха•На§ѓа•Ла§Ва§Ха§њ ৵а•З ু৮а•Л৵а•Иа§Ьа•На§Юৌ৮ড়а§Х а§∞а•В৙ а§Єа•З ৙а•Ба§∞ৌ৮а•А а§єа•Л а§Ьৌ১а•А а§єа•Иа§Ва•§ а§За§Є ৙а•На§∞а§Ха§Ња§∞ а§Ѓа§Ња§Ва§Ч а§Фа§∞ а§Ж৙а•Ва§∞а•Н১ড় а§Ха•А а§ѓа§є ৙а•На§∞а§Ха•На§∞а§ња§ѓа§Њ а§≤а§Ва§ђа•А а§єа•Л১а•А а§Ъа§≤а•А а§Ьৌ১а•А а§єа•Иа•§
а§Й৙а§≠а•Ла§Ха•Н১ৌ৵ৌ৶а•А а§Єа§Ва§Єа•На§Ха•Г১ড় ৮а•З а§ђа§Ња§Ьа§Ња§∞ а§Ха•Л а§Ча§Ња§В৵а•Ла§В а§Ѓа•За§В а§≠а•А ৙৺а•Ба§Ва§Ъа§Њ ৶ড়ৃৌ а§єа•Иа•§ а§ђа§Ња§Ьа§Ња§∞ а§Ха•А а§Єа§Ва§Єа•На§Ха•Г১ড় ৮а•З а§Єа•Ма§В৶а§∞а•На§ѓ а§Ха•З а§Єа§В৵а•З৶ৌ৮ৌ১а•На§Ѓа§Х а§Ѓа•Ва§≤а•На§ѓ а§Ха•Л ৵ড়৪а•НвАН৕ৌ৙ড়১ а§Ха§∞ а§Й১а•Н১а•За§Ь৮ৌ১а•На§Ѓа§Х а§Ѓа•Ва§≤а•На§ѓ а§Ха•Л ৙а•На§∞১ড়ৣа•Н৆ড়১ а§Ха§∞৮а•З а§Ха§Њ ৙а•На§∞а§ѓа§Ња§Є а§Ха§ња§ѓа§Њ а§єа•Иа•§ а§ђа§Ња§Ьа§Ља§Ња§∞ а§Ха§Њ а§Ж৶а§∞а•Н৴ ৵৺ ৮৺а•Аа§В а§єа•И, а§Ьа§єа§Ња§В ু৮а•Ба§Ја•На§ѓ а§Е৙৮а•А а§ђа•Б৮ড়ৃৌ৶а•А а§Ьа§∞а•Ва§∞১ а§Ха•А а§Ъа•Аа§Ьа•Ла§В а§Ха•Л а§За§Ха§Яа•Н৆ৌ а§Ха§∞৮а•З а§Ха•З а§≤а§ња§П а§Ьৌ১ৌ ৕ৌ, а§Ьа§ња§Єа§Ха•З а§≤а§ња§П а§Ча§Ља§Ња§≤а§ња§ђ ৮а•З а§Ха§єа§Њ ৕ৌ- а§Фа§∞ а§ђа§Ња§Ьа§Ља§Ња§∞ а§Єа•З а§≤а•З а§Жа§Па§Ва§Ча•З а§Ча§∞ а§Яа•Ва§Я а§Ча§ѓа§Њ, а§Ьа§Ња§Ѓа•З а§Ьа§Ѓ а§Єа•З а§Ѓа•За§∞а§Њ а§ѓа•З а§Ьа§Ња§Ѓа•З а§Єа§ња§Ђа§Ња§≤ а§Еа§Ъа•На§Ыа§Њ а§єа•И, а§ђа§≤а•На§Ха§њ а§ѓа§є ৵৺ а§ђа§Ња§Ьа§Ља§Ња§∞ а§єа•И, а§Ьа§єа§Ња§В а§єа§∞ а§Ха•Ба§Ы а§ђа§ња§Ха§Ња§К а§єа•Иа•§ а§Ж৙ ৙а•Иа§Єа•З а§Ца§∞а•На§Ъ а§Ха•Аа§Ьа§ња§П, а§Ж৙৪а•З а§°а•За§Яа§ња§Ва§Ч, а§Ъа•Иа§Яа§ња§Ва§Ч а§Фа§∞ ৙а•На§ѓа§Ња§∞ а§Ха§∞৮а•З а§Ха•З а§≤а§ња§П ৙ৌа§∞а•На§Я৮а§∞ а§Ѓа•Ма§Ьа•В৶ а§єа•Иа•§ а§За§Є ১ড়а§≤а§ња§Єа•На§Ѓа•А а§Ѓа§Ња§ѓа§Ња§≤а•Ла§Х а§Ѓа•За§В ুৌ৮৵а•Аа§ѓ а§≠ৌ৵৮ৌа§Па§В а§Фа§∞ а§Єа§В৵а•З৶৮ৌа§Па§В а§Єа§ђ а§Ха•Ба§Ы а§ђа§ња§Х১а•А а§єа•Иа§Ва•§ а§Ча§Ља§Ња§≤а§ња§ђ а§Ха•З а§єа•А ৴৐а•Н৶а•Ла§В а§Ѓа•За§В-а§За§Є а§ђа§Ња§Ьа§Ља§Ња§∞ а§Ха•З а§≤а§ња§П а§Ха§є а§Єа§Х১а•З а§єа•Иа§В, а§≤а•З а§Жа§Па§Ва§Ча•З а§ђа§Ња§Ьа§Ља§Ња§∞ а§Єа•З а§Ьа§Ња§Ха§∞ ৶ড়а§≤-а§У-а§Ьа§Ња§В а§Фа§∞, а§≤а•Ла§Х১ৌа§В১а•На§∞а§ња§Х а§Фа§∞ ৮а•И১ড়а§Х а§Е৵ুа•Ва§≤а•Нৃ৮ а§Ха•З а§Ѓа•Ма§Ьа•В৶ৌ ৶а•Ма§∞ а§Ѓа•За§В а§Ьа§єа§Ња§В ৵ড়а§Ьа•На§Юৌ৙৮-৮ড়а§∞а•Нুৌ১ৌа§Уа§В а§Ха•А а§ѓа§є а§Ьа§ња§Ѓа•На§Ѓа•З৶ৌа§∞а•А ৐৮১а•А а§єа•И а§Ха§њ ৵а•З ৶ড়а§Ча•НвАНа§≠а•На§∞ুড়১ а§Ха§∞৮а•З ৵ৌа§≤а•З а§Фа§∞ а§Ыа§ња§Ыа•Ла§∞а•З а§Ха§ња§Єа•На§Ѓ а§Ха•З ৵ড়а§Ьа•На§Юৌ৙৮а•Ла§В а§Ха•Л ৶а§∞а•Н৴а§Ха•Ла§В а§Ха•З ৪ৌু৮а•З ৮ ৙а§∞а•Ла§Єа•За§В, ৵৺а•Аа§В ৶а§∞а•Н৴а§Ха•Ла§В а§Ха•Л а§≠а•А а§ѓа§є а§Ьа§ња§Ѓа•На§Ѓа•З৶ৌа§∞а•А ৐৮১а•А а§єа•И а§Ха§њ ৵৺ а§Ра§Єа•З ৵ড়а§Ьа•На§Юৌ৙৮а•Ла§В а§Ха•Л ৶а•За§Ца§Ха§∞ а§≠а•А а§Й৮৪а•З ৙а•На§∞а§≠ৌ৵ড়১ ৮ а§єа•Ла§Ва•§ ৵а•З а§Е৙৮а•З а§Ж৙ а§Єа•З а§ѓа§є ৪৵ৌа§≤ а§Ха§∞а•За§В а§Ха§њ а§Ьа§ња§Є ৵ড়а§Ьа•На§Юৌ৙৮ а§Ха•Л ৵৺ ৙৥৊ а§∞а§єа§Њ а§єа•И а§ѓа§Њ ৶а•За§Ц а§∞а§єа§Њ а§єа•И, а§Йа§Єа§Ѓа•За§В а§Єа§Ъа•На§Ъа§Ња§И а§Ха§Њ а§Хড়১৮ৌ а§Еа§В৴ а§єа•И? а§Єа§∞а§Ха§Ња§∞ а§Ха•Л а§≠а•А ৵ড়а§Ьа•На§Юৌ৙৮ а§Ха§В৙৮ড়ৃа•Ла§В а§Ха•З ৵ড়а§Ьа•На§Юৌ৙৮а•Ла§В ৙а§∞ а§Ха§ња§П а§Ьৌ৮а•З ৵ৌа§≤а•З а§Еа§∞а§ђа•Ла§В а§∞а•В৙ৃа•Ла§В а§Ха•Л ৮ড়ৃа§В১а•На§∞ড়১ а§Ха§∞৮ৌ а§Ъа§Ња§єа§ња§П а§Фа§∞ а§Й৮а•На§єа•За§В а§Ѓа•Ба§Ђа•Н১ ৴ড়а§Ха•На§Ја§Њ а§Фа§∞ а§Єа•Н৵ৌ৪а•НвАН৕а•На§ѓ а§Єа§Ва§ђа§Ва§Іа•А а§Єа•З৵ৌа§Уа§В а§Ха•З а§≤а§ња§П ৙а•На§∞а§ѓа•Ба§Ха•Н১ а§Ха§∞৮ৌ а§Ъа§Ња§єа§ња§Па•§ а§Жа§Ь а§Ха•З ু৮а•Ба§Ја•На§ѓ а§Ха•Л а§Е৙৮а•А а§За§Ъа•На§Ыа§Њ а§Фа§∞ а§Ьа§∞а•Ва§∞১ а§Ѓа•За§В а§Ђа§∞а•На§Х а§Ха§∞৮ৌ а§єа•Ла§Ча§Њ, ১а§≠а•А ৵৺ ৵а•На§ѓа§Ха•Н১ড় а§Єа•З ৵৪а•Н১а•Б а§Ѓа•За§В ১৐а•Н৶а•Аа§≤ а§єа•Л৮а•З а§Єа•З а§ђа§Ъ ৙ৌа§Па§Ча§Ња•§ а§Ь৮৪১а•Н১ৌ а§Єа•З а§Єа§Ња§≠а§Ња§∞а•§

 а§Ѓа§Іа•На§ѓ ৙а•На§∞৶а•З৴
а§Ѓа§Іа•На§ѓ ৙а•На§∞৶а•З৴ 





















